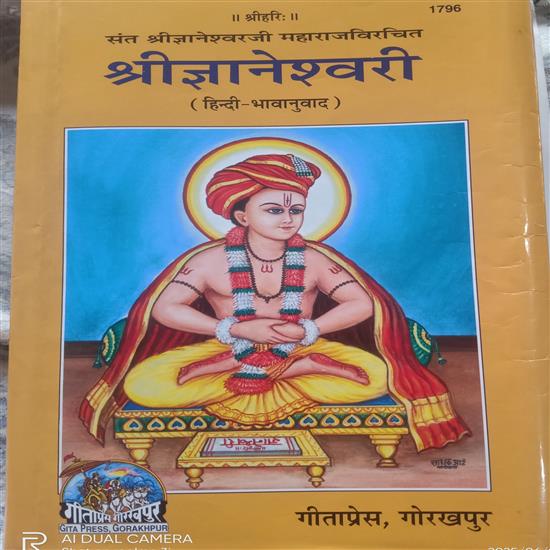अध्याय सोलहवा
अपने अन्तःकरणमें स्वयं सेवक-भावकी परिकल्पना करके शाब्दिक स्तोत्रके साजसे सुसज्जित कर रहा हूँ। यदि मैं यह कहूँ कि आप इस सज्जाको स्वीकार करें तो इस प्रकारकी बात भी अद्वैत आनन्दमें न्यूनतालानेकी ही भाँति होगी। पर जैसे अमृत-सिन्धुके दर्शन होनेपर कोई निर्धन हक्का-बक्का हो जाता है और अपनी योग्यता-अयोग्यताका विचार भूलकर उस अमृत-सिन्धुका आतिथ्य शाक-भाजीसे ही करनेका उपक्रम करने लग जाता है और ऐसे अवसरपर जिस प्रकार उस शाक-भाजीका ही स्वागत करके उस अमृत-सिन्धुके लिये उस निर्धनके आनन्दोल्लासका ही ध्यान रखना समीचीन होता है, ठीक वैसे ही यदि आप भी अपना दिव्य तेज छिपाकर मेरी भक्तिकी इस साधारण आरतीकी ही ओर ध्यान दें, तो मेरा सारा-का-सारा काम सम्पन्न हो जायगा। यदि छोटा बच्चा ही उचित क्या है और अनुचित क्या है, इस बातको अच्छी तरहसे समझ ले तो फिर उसका बचपना ही कहाँ रह जाय ? पर फिर भी उसकी माता उसकी अटपटी बातोंसे सन्तुष्ट होती है अथवा नहीं? जिस समय किसी नालेका जल आकर गंगाके पीछे लग जाता है, उस समय क्या गंगा कभी यह कहकर उसे पीछे लौटा देती है कि दूर हट ? हे देव! भृगु ऋषिने भगवान्के वक्षपर चरण-प्रहार कर कितना बड़ा अपकार किया था! पर उसी चरण-चिह्नको भूषण मानकर उसकी महत्तासे शार्ङ्गधरभगवान् सन्तोष ही मानते हैं न ? अथवा जिस समय अन्धकारसे परिपूर्ण आकाश सूर्यके समक्ष आता है, उस समय क्या सूर्य कभी यह कहकर उसका अपमान करता है कि दूर हट ? ठीक वैसे ही यदि किसी अवसरपर भेद-बुद्धिके चक्करमें पड़कर तथा सूर्यके रूपकका तराजू खड़ा करके मैंने सूर्यके साथ आपकी तुलना की हो, तो हे गुरुदेव ! आप कृपा कर एक बार उस तुलनाको भी सहन कर लें। जिन्होंने ध्यान तथा समाधिरूपी नेत्रोंके द्वारा आपके दर्शन किये हैं और जिस वेद-वाणीने आपका वर्णन किया है, उनके सारे कृत्य आपने जैसे सहन किये हैं, यदि वैसे ही इसे भी आप सहन कर लें तथा उसी न्यायका मेरे लिये भी प्रयोग करें तो काम हो जायगा। हे महाराज! आज मैं जो आपका गुणगान करने लगा हूँ, आप इसे मेरा अपराध न मानें।
आप जी चाहें, सो करें, पर मैं आपके गुणोंका वर्णन करनेका काम तब
तक नहीं बन्द करूँगा, जबतक मेरा जी इस कामसे भर न जायगा। ज्यों ही मैं गीता नामक आपके इस प्रसादरूपी अमृतका बड़े उत्साहसे वर्णन करने लगा हूँ, त्यों ही सौभाग्यवशात् मुझे द्विगुणित बल प्राप्त हो गया है। मेरी वाचाने अनेक कल्पोंतक सत्य बोलनेके तपका आचरण किया था और हे प्रभु! आज वह इसी तपस्याका अनन्त फल प्राप्त कर रही है। आजतक मैंने किसी ऐसे असाधारण पुण्यका सम्पादन किया था और उसीने आज आपका गुणगान करनेकी बुद्धि प्रदान कर मुझे इस कार्यमें उत्तीर्ण किया है। मैं इस जीवावस्थारूपी अरण्यमें घुसकर मृत्युरूपी गाँवमें फँस गया था, पर वह दुर्दशाका चक्कर एकदम मिट गया है। कारण यह है कि आपकी जो कीर्ति गीताके नामसे विख्यात है और जो इस विश्वाभासको पूर्णतया विनष्ट कर देती है, आपकी उसी कीर्तिका विवेचन मेरे हिस्सेमें आया है। क्या उस व्यक्तिको कभी दरिद्र कहा जा सकता है, जिसके घरमें महालक्ष्मी स्वयं ही आसन लगाकर बैठ जायँ ? अथवा यदि सूर्य स्वयं ही अन्धकारके घरमें अतिथिके रूपमें आ पहुँचे तो क्या वह अन्धकार ही इस जगत्में प्रकाश नहीं बन जायगा ? जिस देवके पासंगमें यह अपरम्पार विश्व परमाणुके बराबर भी नहीं टिकता, वही देव यदि भक्तिकी तरंगोंमें आ पड़ें तो फिर वे भक्तके लिये भला कौन-सा रूप नहीं ग्रहण करते? ठीक इसी प्रकार गीताका निरूपण करना आकाश-कुसुमकी सुगन्ध लेनेके सदृश ही असम्भव है; पर आप सामर्थ्यवान् हैं इसलिये आपने मेरी वह इच्छा भी पूरी कर दी है। इसीलिये आपका यह शिष्य ज्ञानदेव भी कहता है कि हे गुरुदेव ! आपकी कृपासे मैं गीताके गूढ़तर श्लोकार्थ भी बहुत ही स्पष्ट और सरल करके निवेदन करूँगा। पिछले यानी पंद्रहवें अध्यायमें भगवान्ने अर्जुनको सम्पूर्ण शास्त्रीय सिद्धान्त स्पष्ट करके समझाये थे। जैसे कोई सवैद्य किसी रोगग्रस्त व्यक्तिके अंगोण प्रविष्ट रोगोंका निदान करता है, वैसे ही वृक्षके रूपकके द्वारा भगवान्ने आलंकारिक भाषामें उपाधिरूपी समस्त विश्वका निरूपण किया